भारतीय सिनेमा, जिसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, और अन्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों के रूप में जाना जाता है, न केवल मनोरंजन का एक माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों का दर्पण भी है। यह समाज के बदलते मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है और कई बार सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित भी करता है। हालांकि, भारतीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण की यात्रा धीमी और जटिल रही है। इस लेख में, हम इस यात्रा को ऐतिहासिक, सामाजिक और समकालीन दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे, जिसमें तथ्यों की जांच, प्रासंगिक घटनाओं और शोधों का उल्लेख होगा।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में महिलाएं
भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में दादासाहेब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई थी। इस दौर में, सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य थी। सामाजिक रूढ़ियों के कारण, महिलाओं का फिल्मों में काम करना अस्वीकार्य माना जाता था, और पुरुष अभिनेता ही महिला किरदार निभाते थे। उदाहरण के लिए, राजा हरिश्चंद्र में तारामती का किरदार एक पुरुष ने निभाया था। यह उस समय की सामाजिक मान्यताओं को दर्शाता है, जहां महिलाओं का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश सीमित था।
1920 के दशक में, जब मूक फिल्मों में महिलाएं अभिनय करने लगीं, तो उन्हें सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। अभिनेत्रियां जैसे फातमा बेगम और सुलोचना (रूबी मायर्स) ने इस दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फातमा बेगम को भारत की पहली महिला फिल्म निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1926 में बुलबुले परिस्तान का निर्देशन किया। हालांकि, इन महिलाओं को समाज में "निम्न" दर्जा दिया जाता था, और उनकी उपलब्धियों को व्यापक मान्यता नहीं मिली।
प्रारंभिक चुनौतियां और रूढ़ियां
प्रारंभिक भारतीय सिनेमा में महिलाओं को अक्सर पारंपरिक और पितृसत्तात्मक ढांचे के भीतर चित्रित किया जाता था। वे या तो पवित्र और समर्पित पत्नी के रूप में दिखाई देती थीं या फिर नकारात्मक किरदारों जैसे कि वैंप या कुलटा के रूप में। 1930 और 1940 के दशक की फिल्में, जैसे देवदास (1935), में महिलाओं को मुख्य रूप से पुरुष नायक की कहानी के सहायक के रूप में दर्शाया गया। इस दौर में, महिला किरदारों की गहराई और स्वतंत्रता सीमित थी, जो सामाजिक मानदंडों को प्रतिबिंबित करता था।
हालांकि, कुछ अपवाद भी थे। 1930 के दशक में, अभिनेत्री दुर्गा खोटे ने अमर ज्योति (1936) जैसी फिल्मों में मजबूत और स्वतंत्र महिला किरदार निभाए। लेकिन ये किरदार अपवाद थे, और मुख्यधारा सिनेमा में महिलाओं को ज्यादातर आदर्श पत्नी, मां या बहन के रूप में ही चित्रित किया जाता था।
स्वतंत्रता के बाद: बदलते परिदृश्य और नई चुनौतियां
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, सिनेमा में सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की प्रवृत्ति बढ़ी। इस दौर में, राज कपूर की आवारा (1951) और बिमल रॉय की दो बीघा जमीन (1953) जैसी फिल्मों ने सामाजिक असमानता और गरीबी जैसे मुद्दों को उजागर किया। हालांकि, इन फिल्मों में भी महिलाएं ज्यादातर सहायक भूमिकाओं तक सीमित रहीं।
इस दौर में, नर्गिस, मीना कुमारी और मधुबाला जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का दिल जीता। नर्गिस ने मदर इंडिया (1957) में राधा के किरदार के माध्यम से एक मजबूत, स्वतंत्र और बलिदानी मां की छवि प्रस्तुत की। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर थी, क्योंकि इसने पहली बार एक महिला किरदार को कहानी का केंद्र बनाया। हालांकि, राधा का किरदार पितृसत्तात्मक ढांचे के भीतर ही था, जहां उसका बलिदान परिवार और समाज के लिए था।
महिला सशक्तिकरण की शुरुआत: समानांतर सिनेमा
1970 और 1980 के दशक में समानांतर सिनेमा का उदय हुआ, जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए नए रास्ते खोले। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और सई परांजपे जैसे निर्देशकों ने महिलाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर फिल्में बनाईं। सई परांजपे की स्पर्श (1980) और चश्मे बद्दूर (1981) ने महिलाओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया। श्याम बेनेगल की अंकुर (1974) और मंडी (1983) ने ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के संघर्षों को दर्शाया।
इस दौर में, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों ने अपने अभिनय से सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी। स्मिता पाटिल की भूमिका (1977) में उदिता का किरदार एक ऐसी महिला का था, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करती है। ये फिल्में न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती थीं, बल्कि समाज में गहरे बैठे लैंगिक भेदभाव को भी उजागर करती थीं।
समकालीन सिनेमा: प्रगति और बाधाएं
21वीं सदी में, भारतीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण की कहानियां अधिक प्रमुखता से उभरीं। कहानी (2012), क्वीन (2014), और मर्दानी (2014) जैसी फिल्मों ने महिलाओं को स्वतंत्र, साहसी और आत्मनिर्भर के रूप में चित्रित किया। विद्या बालन की कहानी में विद्या बागची का किरदार एक गर्भवती महिला का था, जो अपने पति की तलाश में कोलकाता की गलियों में अकेले संघर्ष करती है। यह किरदार न केवल शारीरिक रूप से सक्षम था, बल्कि मानसिक रूप से भी दृढ़ था।
इसी तरह, क्वीन में कंगना रनौत ने रानी के किरदार के माध्यम से एक ऐसी महिला की कहानी पेश की, जो अपनी शादी टूटने के बाद आत्म-खोज की यात्रा पर निकलती है। ये फिल्में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक संदेश भी दिया कि महिलाएं अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकती हैं।
क्षेत्रीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण
क्षेत्रीय सिनेमा, विशेष रूप से मलयालम, तमिल और मराठी सिनेमा, ने भी महिला सशक्तिकरण की कहानियों को बढ़ावा दिया है। मलयालम फिल्म हाउ ओल्ड आर यू (2014) ने मंजू वारियर को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाती है। तमिल फिल्म 36 वैयाधिनीले (2015) ने भी इसी तरह की थीम को अपनाया, जिसमें ज्योतिका ने एक मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी की कहानी को जीवंत किया, जो अपनी पहचान को फिर से खोजती है।
मराठी सिनेमा में, सैराट (2016) ने जातिगत और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को उठाया। हालांकि, इस फिल्म का अंत दुखद था, लेकिन इसने सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह करने वाली एक मजबूत महिला किरदार, आर्ची, को प्रस्तुत किया।
महिला सशक्तिकरण के सामने चुनौतियां
हालांकि भारतीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन। बॉलीवुड की कई व्यावसायिक फिल्में, जैसे कबीर सिंह (2019), में महिलाओं को पुरुष नायक की कहानी के सहायक के रूप में चित्रित किया गया। इस फिल्म की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इसने एक अपमानजनक और नियंत्रित करने वाले पुरुष किरदार को महिमामंडित किया, जबकि महिला किरदार को निष्क्रिय और कमजोर दिखाया गया।
दूसरी चुनौती है स्क्रीन टाइम और किरदारों की गहराई। एक अध्ययन के अनुसार, 2010 से 2020 के बीच बॉलीवुड की शीर्ष 100 फिल्मों में केवल 15% फिल्मों में महिलाएं मुख्य किरदार थीं। अधिकांश फिल्मों में, पुरुष किरदारों को अधिक स्क्रीन टाइम और जटिल कहानियां दी जाती हैं, जबकि महिला किरदारों को सहायक भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता है।
महिला निर्देशकों और लेखकों की कमी
भारतीय सिनेमा में महिला निर्देशकों और लेखकों की संख्या अभी भी बहुत कम है। 2020 में किए गए एक शोध के अनुसार, बॉलीवुड में केवल 12% फिल्में महिलाओं द्वारा निर्देशित थीं। मेघना गुलजार (राजी, 2018), जोया अख्तर (गली बॉय, 2019), और अनुभव सिन्हा जैसे कुछ निर्देशकों ने महिलाओं के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है, लेकिन उद्योग में पुरुषों का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है।
महिला लेखकों की कमी के कारण, कई बार महिला किरदारों की कहानियां पुरुष दृष्टिकोण से लिखी जाती हैं, जिससे उनकी गहराई और प्रामाणिकता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, पद्मावत (2018) में रानी पद्मावती का किरदार ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का था, लेकिन उनकी कहानी को पुरुष निर्देशक के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया, जिससे कुछ आलोचकों ने इसे एक सतही चित्रण माना।
हाल की घटनाएं और तथ्य सत्यापन
हाल के वर्षों में, भारतीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई घटनाएं और चर्चाएं सामने आई हैं। 2018 में #MeToo आंदोलन ने भारतीय फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों को उजागर किया। कई अभिनेत्रियों, जैसे तनुश्री दत्ता और कंगना रनौत, ने उद्योग में यौन शोषण और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसने उद्योग में एक बड़ी बहस छेड़ दी। हालांकि, इस आंदोलन के बाद ठोस बदलाव की कमी ने कई लोगों को निराश किया।
2023 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा (2016) जैसी फिल्मों पर सेंसरशिप के मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा। इस फिल्म को शुरू में रिलीज करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इसमें महिलाओं की यौन इच्छाओं को खुलकर दर्शाया गया था। इस तरह की सेंसरशिप से पता चलता है कि भारतीय समाज अभी भी महिलाओं की स्वतंत्रता और उनकी कहानियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।
शोध और आंकड़े
2021 में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय सिनेमा में लैंगिक समानता की कमी एक वैश्विक समस्या का हिस्सा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व सिनेमा में केवल 20% फिल्में महिलाओं द्वारा निर्देशित होती हैं, और भारत में यह आंकड़ा और भी कम है। इसके अलावा, 2019 में जेंडर स्टडीज जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि बॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं को अक्सर उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर ही चित्रित किया जाता है, न कि उनकी बौद्धिक या भावनात्मक क्षमताओं के आधार पर।
एक अन्य शोध, जो 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया, ने दिखाया कि भारतीय सिनेमा में महिला किरदारों को ज्यादातर पारंपरिक भूमिकाओं (पत्नी, मां, प्रेमिका) में ही दिखाया जाता है। केवल 10% फिल्मों में महिलाओं को पेशेवर या नेतृत्वकारी भूमिकाओं में दर्शाया गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सिनेमा में अभी भी लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने की जरूरत है।
छिपे हुए सत्य और सामाजिक प्रभाव
भारतीय सिनेमा का सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि यह देश की एक बड़ी आबादी के लिए प्रेरणा और मनोरंजन का स्रोत है। हालांकि, सिनेमा में महिलाओं के चित्रण से कई बार सामाजिक रूढ़ियां मजबूत होती हैं। उदाहरण के लिए, 2000 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्मों, जैसे हम तुम (2004) और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), में महिलाओं को प्रेम और परिवार के लिए समर्पित दिखाया गया, जो एक सकारात्मक छवि तो थी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कम ही दर्शाया गया।
दूसरी ओर, कुछ फिल्में जैसे पिंक (2016) और थप्पड़ (2020) ने महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के मुद्दों को उठाया। पिंक में, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू ने यौन सहमति और महिला स्वायत्तता के मुद्दे को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस फिल्म ने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक बहस को भी प्रेरित किया।
महिलाओं का तकनीकी क्षेत्र में योगदान
महिला सशक्तिकरण केवल अभिनय तक सीमित नहीं है। सिनेमा के तकनीकी क्षेत्रों, जैसे संपादन, छायांकन और ध्वनि डिजाइन, में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, गीतांजलि राव ने बॉम्बे रोज (2019) के माध्यम से एनिमेशन और कहानी कहने में अपनी प्रतिभा दिखाई। इसी तरह, रीमा दास ने असमिया सिनेमा में विलेज रॉकस्टार्स (2017) जैसी फिल्मों के साथ वैश्विक पहचान हासिल की।
हालांकि, इन क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। 2020 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि इसके छायांकन और संपादन पाठ्यक्रमों में केवल 25% छात्र महिलाएं थीं। यह दर्शाता है कि तकनीकी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए और प्रयासों की जरूरत है।
भविष्य की संभावनाएं
भारतीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण की यात्रा धीमी रही है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम, ने नई कहानियों और महिला केंद्रित कथानकों को बढ़ावा दिया है। दिल्ली क्राइम (2019) और मसाबा मसाबा (2020) जैसी वेब सीरीज ने महिलाओं को जटिल और प्रामाणिक किरदारों में प्रस्तुत किया है।
इसके अलावा, महिला निर्देशकों और लेखकों की नई पीढ़ी, जैसे कि अनुपमा चोपड़ा और कोंकणा सेन शर्मा, उद्योग में बदलाव ला रही है। इन महिलाओं ने न केवल अपनी रचनात्मकता से प्रभावित किया है, बल्कि लैंगिक समानता के लिए भी आवाज उठाई है।
सुझाव और समाधान
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सिनेमा को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
1. महिला लेखकों और निर्देशकों को प्रोत्साहन: अधिक महिलाओं को कहानी लेखन और निर्देशन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
2. लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण: फिल्म उद्योग में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।
3. विविध किरदारों का निर्माण: महिलाओं को केवल पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित न रखकर, उन्हें वैज्ञानिक, उद्यमी और नेता जैसे किरदारों में दर्शाया जाना चाहिए।
4. सेंसरशिप में सुधार: सेंसर बोर्ड को महिला केंद्रित कहानियों के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारतीय सिनेमा में महिला सशक्तिकरण की यात्रा चुनौतियों और अवसरों से भरी रही है। प्रारंभिक मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक, महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ता से उद्योग में अपनी जगह बनाई है। हालांकि, लैंगिक रूढ़ियों, ऑब्जेक्टिफिकेशन और असमान अवसरों जैसी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं।
भविष्य में, भारतीय सिनेमा को न केवल मनोरंजन का साधन बनना चाहिए, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक मंच भी होना चाहिए। महिलाओं की कहानियों को प्रामाणिकता और सम्मान के साथ प्रस्तुत करके, सिनेमा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकता है। यह यात्रा धीमी हो सकती है, लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम इसे और तेज कर सकते हैं।






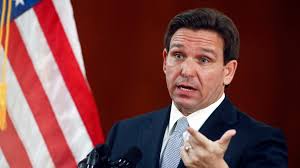



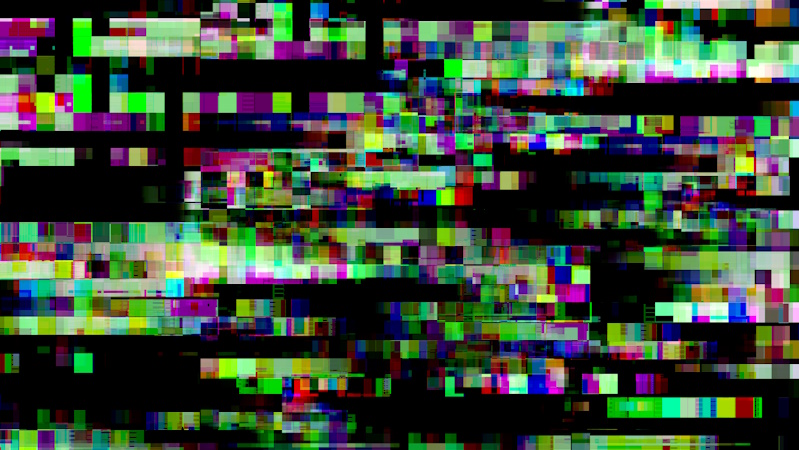

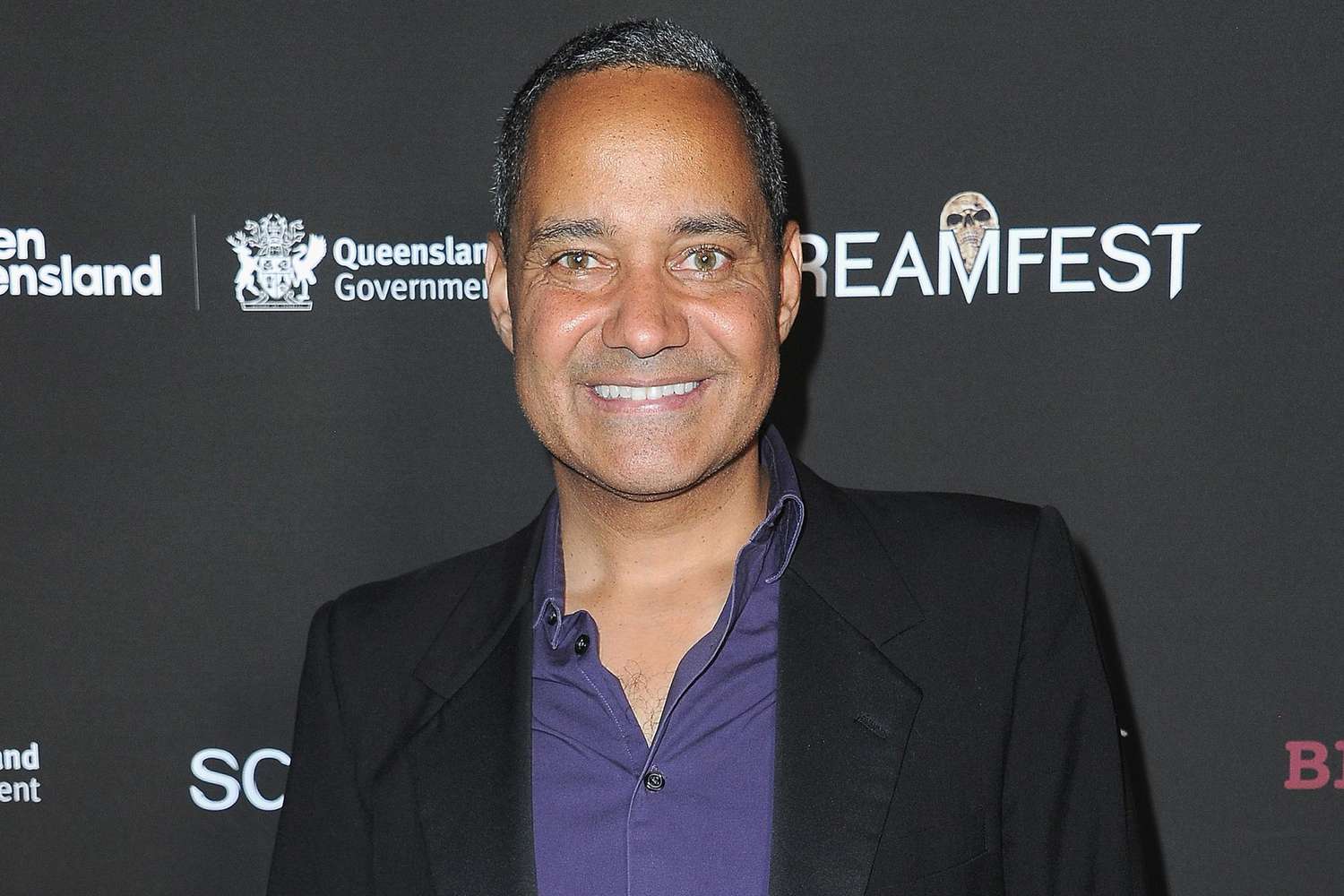












0 Comments